





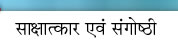
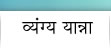
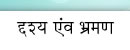
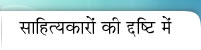

|
परिचयव्यंग्य विधा को पूरी तरह समर्पित प्रेम जनमेजय व्यंग्य- लेखन के परंपरागत विषयों में स्वयं को सीमित करने में विश्वास नहीं करते हैं । उनका मानना है कि व्यंग्य लेखन के अनेक उपमान मैले हो चुके हैं । बहुत आवश्यक है सामाजिक एवं आर्थिक विसंगतियों को पहचानने तथा उनपर दिशायुक्त प्रहार करने की ।व्यंग्य को एक गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले प्रेम जनमेजय आधुनिक हिंदी व्यंग्य की तीसरी पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं । पिछले चौंतिस वर्षों से साहित्य रचना में सृजनरत इस साहित्कार ने हिंदी व्यंग्य को सही दिशा देने में सार्थक भूमिका निभाई है। परंपरागत विषयों से हटकर प्रेम जनमेजय ने समाज में व्याप्त अर्थिक विसंगतियों तथा सांस्कृतिक प्रदूषण को चित्रित किया है । व्यंग्य के प्रति गंभीर एवं सृजनात्मक चिंतन के चलते ही उन्होंनें ‘व्यंग्य यात्रा’ का प्रकाशन आरंभ किया । बहुत कम समय में ही इस पत्रिका ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। यह इस पत्रिका के प्रकाशन का ही परिणाम है कि वर्तमान में व्यंग्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं हो रहीं हैं और सार्थक व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं । विद्वानों ने इसे हिंदी व्यंग्य साहित्य में ‘राग दरबारी’ के बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना माना है । इस पत्रिका को सभी साहित्यकारों का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है । प्रेम जनमेजय ने व्यंग्य-साहित्य में अपने योगदान के अतिरिक्त बाल-साहित्य और नवसाक्षर- लेखन में भी महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाई है । ‘शहद की चोरी’, ‘अगर ऐसा होता’ आदि बाल रचनाओं के कहानी संकलनों तथा ‘नल्लूराम’ जैसे बाल उपन्यास के माध््यम से बालमनोविज्ञान की उनकी गहरी पकड़ को रेखांकित करते हैं ।
जन्म
नाम
प्रथम प्रकाशित कहानी
पहला रेडियो नाटक
पहला व्यंग्य
शिक्षा
व्यवसाय
अन्य संस्थाओं से सम्बद्धता
अन्य
संपादन
सम्प्रति आत्मकथ्यआजकल आत्मा की आवाज की जैसे
सेल लगी हुई है । जिसे देखो वो ही आत्मा की आवाज सुनाने को उधार
खाए बैठा है । आप न भी सुनना चाहें तो जैसे -क्रेडिट कार्ड, बैंकों
के उधारकर्त्ता, मोबाईल कंपनियों के विक्रेता अपनी कोयल-से मधुर
स्वर में आपको अपनी आवाज सुनाने को उधर खाए बैठे होते हैं, वैसे ही
आत्मा की आवाज सुनने-सुनाने का धंधा चल रहा है । कोई भी धार्मिक
चैनल खोल लीजिए, स्वयं अपनी आत्मा को सुला चुके ज्ञानीजन आपकी
आत्मा को जगाने में लगे रहते हैं । आपकी आत्मा को जगाने में उनका
क्या लाभ, प्यारे जिसकी आत्मा मर गई हो वो धरम- करम कहां करता है,
धरम-करम तो जगी आत्मा वाला करता है और धरम-करम होगा तभी तो
धार्मिक-व्यवसाय फलेगा और फूलेगा। इसलिए जैसे इस देश में
भ्रष्टाचार के सरकारी दफतरों में विद्यमान् होने से वातावरण जीवंत
और कर्मशील रहता है वैसे ही आत्मा के शरीर में जगे रहने से ‘धर्म’
जीवंत और कर्मशील रहता है । कबीर के समय में माया ठगिनी थी , आजकल
आत्मा ठगिनी है । माया के मायाजाल को तो आप जान सकते हैं , आत्मा
के आत्मजाल को देवता नहीं जान सके आप क्या चीज हैं । सुना गया है
कि आजकल आत्मा की ठग विद्या को देखकर बनारस के ठगों ने अपनी
दूकानों के शटर बंद कर लिए हैं । आत्मा की आवाज कितनी सुविधाजनक हो
गई है, जब चाहा जगा दिया जब चाहा सुला दिया जैसे घर की बूढ़ी अम्मा
, जब चाहा मातृ- सेवा के नाम पर ,दोस्तों को दिखाने के लिए ड्ाईंग
रूम में बिठा लिया और जब चाहा कोने में पटक दिया ।
प्रत्येक सांसारिक जीव का प्रयत्न तो यही होता है कि अपनी आत्मा को कम -से -कम कष्ट दिया जाए और दूसरे की आत्मा जितनी कष्ट में हो उसका आनंद उठाया जाए। मैं भी सांसारिक जीव हूं और उपर से सोने पर सुहागा ये कि दोयम दर्जे के साहित्य -रचना का पाप-कर्म करने वाला व्यंग्य लेखक हूं। व्यंग्य लेखक तो दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाने का दुष्कर्म करने वाला जाना जाता है। ऐसे में ‘आत्म कथ्य’ लिखवाने के बहाने से, मुझ अकिंचन लेखक की आत्मा के किन अंधेरे कोनों को सार्वजनिक करने की इच्छा संपादक की है, नहीं जानता। हां इतना जरूर जानता हूं कि ‘आत्म कथ्य’, ‘आप क्यों लिखते हैं’, ‘मेरी रचना प्रक्रिया’, ‘गर्दिश के दिन’ जैसे विषयों पर निबंध लिखने के लिए संपादक ऐसे ही लेखकों से कहते हैं जिनके संबंध में वे निश्चित होते हैं कि वह घिसा हुआ लेखक है और साहित्य-संसार की धूल मे लोट- लोट कर बड़ा हो चुका है। ये वैसे ही है जैसे साहित्यिक गोष्ठियों में आपको मुख्य अतिथि या अध््यक्ष के रूप में निमंत्रित कर आपको अहसास दिया जाने लगे कि आप घिसे हुए साहित्यकार हो गए हैं। ऐसे में मेरा कर्तव्य हो जाता है कि संपादक को धन्यवाद दूं कि उसने मुझे भी घिसा हुआ साहित्यकार समझा और मुझसे ‘आत्मकथ्य’ जैसा निबंध लिखने के लिए कहा। जिन दिनों ‘गर्दिश के दिन’ नामक निबंध लिखवाने का दौर चल रहा था मैं भी प्रतीक्षा में था कि कोई मेरी गर्दिशी का हाल भी पूछ लेगा। यहां हाल यह है कि शारीरिक उम्र के साठ वसंत और साहित्यिक उम्र के लगभग चवालिस वसंत देख डाले पर मेरे पतझड़ों का हाल किसी ने न पूछा । हाल कोई पूछे तो तब ही बताया जायेगा । बिना पूछे बताओ तो लोग पागल करार देते हैं । मुझे लगा कि ओ हेनरी की कहानी की तरह अंततः अपना बेहाल मुझे जीवन-तांगे में जुते किसी घोड़े को ही सुनाना होगा । वैसे बाजारवाद और खुली अर्थव्यवस्था के युग में घोड़े भी रेस कोर्स के मैदान में ही अधिक पाये जाते हैं, तांगें तो लालटेन की तरह अतीत की वस्तु हो गए हैं या रईसों के एनटीक प्रेम का शिकार बन किसी सुंदर समुद्र तट पर अटखेलियां करते है। ;आजकल जो रेसीय युग चल रहा है उसमें बेचारे जानवर और कहां पाये जायेंगें । गालिब ने कुछ ऐसा कहा- मौत का एक दिन मुययिन है, नींद पिफर रात भर क्यों नहीं आती। इसी तर्ज पर मुझे लगता है कि गर्दिश के दिन तो किसी तरह भीड़- भाड़ में कट जाते हैं पर गर्दिश की रातें नहीं कटती हैं । पर क्या किया जाये हिन्दी साहित्य में गर्दिश के दिन लिखने का ही फैशन है । वैसे भी लेखक की रातों में किसको दिलचस्पी हो सकती है । यह मेरी मां और बाउजी-स्व0सत्या कुंद्रा और स्व0राम प्रकाश कुंद्रा, की छत्र -छाया का असर रहा कि उन्होंनें अपनी पूरी कोशिशों के साथ स्वयं को गर्दिश की रातों के हवाले कर मेरे गर्दिश के दिनों को मुझसे दूर ही करने का प्रयत्न किया । देश की आजादी के दूसरे वर्ष अर्थात् 1949 में जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता- पिता विभाजन की गर्दिश को इलाहाबाद में झेल रहे थे । इन दिनों कुंद्रा शब्द शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के कारण काफी चर्चित हो रहा है और पेज थ्री के पन्नों पर चमक रहा है। ऐसे में मैं भी बता दूं कि मेरे माता-पिता द्वारा दिया गया मेरा नाम प्रेम प्रकाश कुंद्रा अवश्य है पर मेरा राज कुंद्रा से कोई सबंध नही है। मेरे पिता, स्व0 राम प्रकाश कुंद्रा, ने मुझे बताया था कि मेरे पूर्वज जंड करील के रहने वाले थे और शायद वहॉं से ही कुंद्रा शब्द बना । औलियापुर से जंडियाला, दो व्यक्ति आए । जंडियाला में पांच छह सौ कुंद्रा परिवार थे । वधवामल जो औलियापुर में थे,जिन्हें अंग्रेज भी सलाम करते थे- उन्हें शाह जी कहा जाता था। वो अज्ञानियों को बेवकूफ बनाते थे। जैसे वे कहते- उन्नीस सवाया पौने साठ, तीन छोड़े तो पूरे बासठ । इनके पुत्र खेमामल थे जो जंडियाला में आ गए। खेमामल मेरे परदादा थे। मेरे परदादा के तीन पुत्र थे- नत्थूराम, रतनचंद और अमरचंद। अमरचंद कुंद्रा मेरे दादा थे। मेरे दादा बहुत शाह खर्च थे, पांच रुपए की कमाई और पचास का खर्च यानि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मेरे दादा के तीन बेटे और तीन बेटियां थीं। मेरे पिता रामप्रकाश कुंद्रा सबसे बड़े बेटे थे और अधिकांशतः लाहौर कूचा सेठ में अपनी मासी के पास ही रहे। अपनी पिता की हम तीन संताने हैं- प्रेम,सत्य और शांति। हमारी सबसे छोटी एक बहन का जन्म भी हुआ था जो जन्म लेते ही स्वर्ग सिधर गई। जितना मेरे दादा और पिता ने बताया,उसके आधार पर मेरे परिवार का वंश-वृक्ष निम्नलिखित बनता हैः हम जंड करील के रहने वाले हैं, शायद वहॉं से ही कुन्द्रा शब्द बना है। औलियापुर से जंडियाल दो व्यक्ति आए । जंडियाला में पांच छह सौ परिवार कुंद्रा परिवार थे । वधवामल जो औलियापुर में थे , जिन्हें अंग्रेज भी सलाम करते थे । इनके पुत्र खेमामल थे जो जंडियाला में आ गए । वधवामल
।
रामप्रकाश का विवाह सत्या जुल्का से हुआ, सत्या जुल्का के पिता का
नाम लभ्भूराम था। सत्या जुुल्का सात भाईयों की एकलौती बहन थीं।
रामप्रकाश एवं सत्या की तीन संताने हैं।खेमामल । ------------------------------------------------------- नत्थूराम अमरचंद रतनचंद । रामप्रकाश यशपाल हकूमतराय । ।
। ।
प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम जनमेजय सत्य प्रकाश शांति प्रकाश । । । उज्ज्वल-अभिलाषा, विदित-नेहा पुनीत-शुचिता अनुज श्रुति । । रुचिर हिमांक स्पर्श मेरे माता-पिता ने देश के विभाजन की त्रासदी झेली है। पिता सरकारी नौकरी पर थे और गांव से नौकरी करने लाहौर आते थे। पता चला कि गांव में खून- खराबा हो रहा है और उनके बहुत ही गहरे मुस्लमान दोस्त राशिद ने सलाह दी कि तुम इंडिया चले जाओ। पिता, जो भी गाड़ी मिली उसमें बैठकर भारत आ गए। इस विभाजन के कारण पूरा परिवार बिखर गया। मेरी दादी और बुआ एक साथ थे। का़िफले पर हमला हुआ। दादी मारी गई और मेरी बुआ, शीला विज्रा, जो इस समय शहडोल मे रहती हैं, उस समय छह वर्ष की थीं और उनके सर पर कुल्हाड़ी लगी । वे मेरी मृत दादी के पास खून में लथपथ थीं। तभी वहां कोई मुसलमान आया, उसने देखा कि बच्ची में जान है। उसने मेरी बुआ को उठाया, कुछ दूर चला, फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, मेरी बुआ को पास ही मढ़ैयों श्मशान, में छोड़कर चला गया। अगले दिन फिर आया और देखा कि बच्ची में जान है। उसने उठाया और कुछ दूर जा रहे मिल्ट्री के ट्रक वालों को सौंप दिया। विभाजन की त्रासदियों का वर्णन लगभग एक जैसा ही कष्ट देता है। पर मेरे माता-पिता ने हम भाईयों को कभी उस खून-खराबे के किस्से नहीं सुनाए। मेरी मां तो जब भी अपने बीते दिनों को याद करतीं तो अपनी उन मुस्लिम सहेलियों के प्यार भरे बचपन और किशोरावस्था को याद करती जिनमें स्नेह और प्यार के धागे बंध्ेा हुए थे। उन्होंने हमारे मन में कभी भी नफ़रत के बीज नहीं बोए। मेरे पिता ने तो हम तीनों भाईयों के नाम अपने हिसाब से, बिना किसी पंडित से नाम का अक्षर निकलवाए, एक सार्थक सोच के साथ रखे- प्रेम,सत्य और शांति। वे कहा करते थे कि तुम्हें अपने नाम सार्थक करने हैं। मेरा नाम तो इलाहबाद की गंगा के किनारे, पंडित जी ने त्रिवेणी प्रसाद कुंद्रा रखा था। यही नाम मेरी जन्म- पत्री में भी लिखा हुआ है। मेरे पिता ने कभी अपने नाम के साथ जातिवाचक चिह्न, कुंद्रा, का भी प्रयोग नहीं किया,उनसे संबंधित सभी कागजों में उनका नाम मात्र राम प्रकाश ही लिख हुआ है। इसी परंपरा में उन्होंने मेरे नाम के साथ, मेरे दोनों भाईयों के साथ भी कभी जातिवाचक चिह्न नहीं लिखवाया। स्कूली प्रमाणपत्रों से लेकर कॉलेज के प्रमाणपत्रों तथा कॉेलेज में नौकरी के कागजों में मेरा नाम केवल प्रेम प्रकाश ही लिखा हुआ है। मेरा जन्म इलाहबाद के कमला नेहरू अस्पताल में 18 मार्च, 1949 को दोपहर ढाई बजे हुआ था और मां बताती हैं कि वे मेरे जन्म एक दिन पूर्व चंद्रलेखा फिल्म देखकर आईं थी। उन दिनों हम पैलेस सिनेमा के कहीं पीछे रहते थे। आज भी इलाहबाद का नाम आते मेरे मन भावुक हो जाता है। मेरे शैशव के आरंभिक वर्ष वहीं गुजरे हैं। मुझे कुछ-कुछ अपने, पैलेस सिनेमा के पीछे वाले घर की याद है। इस अतीत का अजब संयोग सन्1966 में दिल्ली में मिला। इलाहबाद के पेैलेस सिनेमा के पीछे वाले घर के पड़ोस में एक सेठी परिवार रहता था। उनके बच्चे हमारे समव्यस्क थे। जब मैंनें हस्तिनापुर कॉलेज में हिंदी आनर्स में प्रवेश लिया तो मेरे पिता ने मुझे बताया कि तुम्हारी क्लास में एक लड़की पड़ती है, कुसुम सेठी, वो इलाहबाद में हमारे पड़ोसी थे। बचपन की मोहब्बत जैसा कुछ नहीं था, फिर भी वो जवानी में मिला। इलाहबाद में पिता मुंह अंधेरे हम भाईयों को गंगा किनारे घुमाने ले जाते थे। वे आरंभ से ही मुंह अंधेरे उठने वाले और जितना हो सके पैदल चलने वाले रहे। मेरे पिताजी को पढ़ने और उसपर चर्चा करने का बहुत शौक था। उन्हें जब बोलास छुटती थी तो उनके लपेटे में आया व्यक्ति बहुत मुश्किल से छूटता था। ऐसे में वे उसे ही पकड़ते थे जो उनकी उम्र,रिश्ते आदि का लिहाज कर चुपचाप सुनता रहता था। मेरे अनेक मित्रों ने उनकी इस बोलास को ‘सहा’ है। सन् 1959 में वे इलाहबाद से, डेपुटेशन पर दिल्ली, सी ए जी आपिफस में क्लर्क के रूप में आए। हर समय उनके सिर पर वापस इलाहबाद जाने की तलवार लटकती रही। उनके मित्र लाख समझाते रहे कि ,सरकारी क्वार्टर कब तक रहेगा, कोई प्लॉट-वलाट ले लो। पिताजीका उत्तर होता- ये तीनों बेटे मेरे मकान हैं। 31 दिसंबर 2002 को 82 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ और मां दो वर्ष तक कैंसर की पीड़ा को भोगने के बाद 8 जून 2008 को 82 वर्ष की आयु में हमंे छोड़ गईं। सभी जीवों के जीवन का वर्णन किसी महाकाव्य से कम वृहद् नहीं होता है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसा होता है। तो इस व्यक्तिगत पक्ष को छोड़कर कुछ साहित्यिक हुआ जाए। मुझ ‘र्निवैष्वणन्’ की साहित्यिक वार्ता सुनी जाए। मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने के स्वतंत्रता-शिशु की गोद में अपनी आंखें खोली और जो इस देश के साथ बड़ा होता हुआ आज बुजुर्ग हो गया है। मेरी पीढ़ी वो पीढ़ी हे जो लालटेन से कंप्यूटर तक की यात्रा की है। मेरी पीढ़ी ने युद्ध और शांति के अध््याय पढ़े हैं, मेरी पीढ़ी ने राशन की पंक्तियों में खड़ी गरीबी देखी है तो चमचमाते मॉलों में, विदेशी ब्रांड के लिए नौजवानों की पागल भीड़ देखी है। मेरी पीढ़ी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा है, हरित क्रांति की हरियाली देखी है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चमचमाते सूदखोर बनिए जैसे गैरराष्ट्रीयकृत बैंक देखे हैं तथा समृद्ध, विदेशी निवेश से चढ़ते शेयर बाजार के सैंसक्स के बीच भारत में आत्महत्या करते हुए किसान भी देखे हैं। मैंनें विश्व में छायी मंदी के बावजूद देश की अर्थ-व्यवस्था की जी डी पी को बड़ते देखा है पर साथ ही ईमानदारी, नैतिकता, करुणा आदि जीवन मूल्यों की मंदी के कारण गरीब की जी डी पी को निरंतर गिरते ही देखा है। जो अपने पिता से पिटी और अपने बच्चों से भी पिटी। जैसे हिन्दी का हर लेखक अपना आरम्भिक लेखकीय जीवन, काव्य लेखन के साथ करने के लिये विवश है, मैंने भी किया । परन्तु कविता के साथ कहानी की भी शुरुआत हो गयी । 1963-1966 के बीच मैं रामकृष्णपुरम् सेक्टर तीन के सरकारी स्कूल की नवीं कक्षा में पढ़ता था और विज्ञान का छात्र था । हमारे अंग्रेजी के अध््यापक श्री बत्तरा के प्रयत्नो के फलस्वरूप पहली बार किसी सरकारी विद्यालय ने अपनी पत्रिका निकालने का स्वप्न पूरा किया । मैंनें उस पत्रिका में,1965 में, अंग्रेजी की एक कविता के माध्यम से, अपना तुच्छ योगदान दिया । कविता जब प्रकाशित होकर आई तो अपनी ही कविता को छपा देखकर तथा उसकी प्रशंसा सुनकर मन और रचानायें लिखने को प्रेरित हुआ । गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं और अध््यापक पढ़ाने में कम तथा अपने रजिस्टर और डायरियां लिखने में अधिक रुचि ले रहे थे । ऐसे में पिछले बैंच में बैठकर मैंनें और मेरे सहपाठी मित्र सुदर्शन शर्मा ने एक कहानी लिखी, ‘छुट्टियां ’ । सुदर्शन अब इस दुनिया में नहीं है और न ही उसके साथ लिखी वह कहानी ही किसी पत्रिका के पन्नों में जिंदा है, पर उसकी यादें आज भी किसी ताजा रचना की तरह जिंदा हैं । विज्ञान की पढ़ाई तथा दोबारा पत्रिका न प्रकाशित होने की विवशता ने उस कहानी को किसी अनाम कोने में जैसे गुम कर दिया , पर मेरे अंदर लिखने का इच्छा अपने पंख तलाशती रही । ग्यारवीं की परीक्षा देने के बाद मेर पास कुछ करने को न था । बात 1966 की है । उन दिनों इंजीयनियरिंग आदि की परीक्षाओं के लिए गर्मियों की छुट्टियों का बलिदान नहीं करना पड़ता था। मेरे अंदर का लेखक फिर जागा और मैंनें एक प्रेम-कथा लिखी-- कल आज और कल । इसे मैंनें गाजियाबाद से उन दिनों अपने शीघ्र प्रकाशन की घोषणा करने वाली पत्रिका ‘ खिलते फूल’ में भेज दिया । इधर हायर सैकेंडरी का परिणाम आया और मैंनें दिल्ली विश्वविद्यालय के आज के कॉलेज ‘मोती लाल नेहरू कॉलेज’,और इससे पूर्व डिग्री कॉलेज के रूप में और बाद में हस्तिनापुर कॉलेज के नाम से जाना गया, में गणित आनर्स में प्रवेश लिया। उन्हीं दिनों मेरी कहानी भी ‘खिलते फूल’ में प्रकाशित होकर आ गई। यह कहानी मैंनें प्रेम प्रकाश ‘शैल’ के नाम से लिखी थी। मैंनें यह कहानी उस समय हिंदी विभाग के अध््यक्ष महेंद्र कुमार को दिखाई। वे उन दिनों हिंदी आनर्स कोर्स आरंभ करने के लिए विद्यार्थी जुटा रहे थे। मैं उन्हें सुपात्र लगा और उन्होंने मुझे हिंदी आनर्स के लिए लगभग धकेलना आरंभ किया। मैंनें जब कहा कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं और मैंनें तीन वर्ष तक हिंदी को छुआ तक नहीं है तो उन्होनें कहा कि मैंनें बी0 एससी के बाद एम0 एम0 हिंदी की है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके विभाग के एक अध््यापक नरेंद्र कोहली ने भी विज्ञान के बाद हिंदी आनर्स किया है। सन् 1966 में हिंदी के लिए अंादोलन भी चल रहे थे। अनेक कारण एकत्रित हुए और मैंनें हिंदी आनर्स में प्रवेश ले ही लिया। नरेन्द्र कोहली और कैलाश वाजपेयी जैसे लेखकों को गुरु के रूप में पाने पर मेरे लेखक-मन की बलवती इच्छा ने भी इसमें प्रबल योगदान दिया। धीरे-धीरे कहानी,कविता लिखना, विभिन्न प्रतियोगिताओं में जाना, पुरस्कार प्राप्त करना जैसे मेरे जीवन का अंग बन गया । इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन साहित्यिक माहौल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ‘धर्मयुग’ का बैठे ठाले और साप्ताहिक हिंदुस्तान का ‘ताल बेताल’ स्तंभ पहली पसंद बन गये । परसाई,जोशी और त्यागी की तिकड़ी का हास्य-व्यंग्य लेखन अपने रंग में रंगने लगा। उन दिनों टाईम्स ग्रुप की फिल्मी पत्रिका ‘माधुरी’ में मेरे व्यंग्य यदा-कदा प्रकाशित होने लगे । उन दिनों कैलाश वाजपेयी के प्रभाव में मैंनें आध्ुनिक कविताएं लिखीं तो एम0ए0 में प्रसाद स्पेशल होने के कारण छायावादी प्रभाव की कविताएं भी लिखीं । नरेंद्र कोहली के गद्य-व्यक्तित्व ने मुझे आकर्षित किया ओर उन्होंने जो आत्मीय-समय दिया उसने मुझे उनके बहुत करीब भी किया । हरिशंकर परसाई के लेखन से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और उनकी व्यंग्य सम्बन्धी मान्यताओं से लगभग सहमत । परसाई में विसंगतियों को लक्षितकर उनकी दृष्टिसम्पन्न विश्लेषणात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति ने मेरे व्यंग्य -लेखन को और गति दी । मैनें सन् 1969 में हस्तिनापुर कॉलेज, जो आजकल मोती लाल नेहरू कॉलेज के नाम से जाना जाता है, बी0 ए0 हिंदी आनर्स किया। विभिन्न कॉलेजों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के कारण विश्वविद्यालय की साहित्यिक गतिविध्यिों से मैं बखूबी परिचित था,और लोग मेरे लेखकीय कर्म से परिचित हो रहे थे। प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए कॉलेज स्तर पर हमें बकायदा तैयार किया जाता था। कहानी या वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना हो तो नरेंद्र कोहली तैयारी करवाते थे और यदि कविता प्रतियोगिता हो तो कैलाश वाजपेयी तैयारी करवाते थे । कैम्पस के प्रतियोगियों के होते हुए कोई पुरस्कार पा लेना शेर के मुंह से शिकार छीन लेने के बराबर होता था। नरेंद्र कोहली का मेरे लेखकीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लेखन उनके लिए मिशन है, जनून है और जीवन की प्राथमिकता है। लेखक के रूप में प्रेमचंद उनके आदर्श हैं। लेखन को प्राथमिकता देने का संस्कार नरेंद्र कोहली ने प्रेमचंद के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सुदृढ़ किया है। हमारे विद्यार्थी काल में वे अक्सर प्रेमचंद के उदाहरण देते थे। जैसे कि प्रेमचंद एक हाथ से लिख रहे हैं और दूसरे से गोद में बैठे बच्चे को थपका भी रहे हैं। नरेंद्र कोहली अपने आरंभिक काल में न केवल अपने लेखन के प्रति सजग रहे अपितु उन नवलेखकों के भी सजग- सहायक रहे जो घुटनों चलना सीख रहे थे। नए लेखकों की रचनाओं को गंभीरता से ठीक करना, उनके भाषा दोषों को सुधरना। नरेंद्र कोहली ने ये परंपरा अपने गुरु चंद्रभूषण सिन्हा से ग्रहण की। इसी परंपरा के तहत उन्होंनें कॉलेज में लेखक-मंडल की गोष्ठियां आरंभ की। इसी परंपरा को मैंनें त्रिनिदाद में अपने प्रवास के दौरान शुरु किया। इन गोष्ठियों में अधिकांशतः हिंदी आनर्स के ही छात्र थे। लेखक-मंडल की गोष्ठी के स्थायी अध्यक्ष नरेंद्र कोहली होते थे। गोष्ठी में शामिल होने वाले रचनाकार के लिए शर्त थी कि वह अपनी नई रचना लेकर आएगा, उसका पाठ करेगा, तत्पश्चात् सभी अपनी तरह से प्रतिक्रिया जाहिर करेंगें और हो सकेगा तो सुझाव देंगे तथा अंत में नरेंद्र कोहली रचना का ‘छिद्रान्वेषण’ करते। आरंभ में कुछ गोष्ठियां कॉलेज में हुईं परंतु व्यवस्था ठीक न लगने के कारण तथा लड़कियों के देर तक न रुक पाने के कारण ये गोष्ठियां रविवार को नरेंद्र कोहली के तत्कालीन निवास-स्थान एस-362 ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 दिल्ली में होने लगीं। गोष्ठी का समय समान्यतः 9 बजे होता पर दस बजे के लगभग ही गोष्ठी आरंभ हो पाती । आरंभ में इन गोष्ठियों में हस्तिनापुर कॉलेज से जुड़े लेखक ही होते। कुछ के नाम मुझे याद हैं- वीणा, रंजना,सुमन, जोगेंद्र सिंह, कुसुम, सुरेश कांत, राजेश कुमार, हरिमोहन, दिनेश कपूर आदि। बाद में लोग जुड़ते और बिछुड़ते गए। इन गोष्ठियों में दिविक रमेश, सुध्ीश पचौरी, क्षमा शर्मा,रमेश बतरा, मीरा सीकरी, तेजेंद्र शर्मा,गीता विज, शैलेंद्र, आशा जोशी, रमेश ठगेला आदि भी आते-जाते रहे। मैं निरंतर इन गोष्ठियों में शामिल रहा। कई बार तो, किसी-किसी गोष्ठी में मैं नरेंद्र कोहली और उनकी पत्नी मधुरिमा कोहली ही होते। इन गोष्ठियों का लाभ ये हुआ कि गोष्ठी के लिए नई रचना लिखने का दबाव रहता, नरेंद्र कोहली के पास आने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं को पढ़ने का सुअवसर मिलता और रचनाएं प्रकाशनार्थ किन पत्रिकाओं में भेजी जा सकती हैं, इसका परामर्श मिलता। नरेंद्र कोहली ने चाहे अपने लेखन का आरंभ कविताओं से किया परंतु बहुत जल्दी उनका गद्यकार उनपर हावी हो गया और इतना कि नई कविता की इस हद तक कटु आलोचना करने लगा कि नए कवि ‘लेखक मंडल’ की गोष्ठी में आने से कतराने लगे। मैं कतरया तो नहीं पर गद्य की ओर प्रमुखता से मुढ़ गया। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली कविता-प्रतियोगिताओं के लिए या वैसे ही मैं कोई कविता लिखता तो उसे कैलाश वाजपेयी को दिखाता और उनसे परामर्श लेता। कैलाश वाजपेयी के प्रभाव में मैंनें अनेक कविताएं लिखीं। लेखक मंडलीय गोष्ठी के आरंभिक दौर में मैं रामकृष्ण पुरम् के सेक्टर-1 के सरकारी क्वार्टर न0 833 में अपने पिता को मिले सरकारी क्वार्टर में रहता था। हमारे पड़ोस मे, शायद 839 में आज के प्रसिद्ध कथाकार विजय रहा करते थे। आरंभ में मैंनें प्रेम प्रकाश ‘निर्मल’, प्रेम प्रकाश ‘शैल’ तथा परीक्षित कुंद्रा के नाम से कहानियां लिखीं जिनमें ‘कल आज और कल’ , ‘अभिव्यक्ति’ ‘समुद्र’ ‘बस स्टॉप की भीड़’ आदि हैं। प्रसाद मेरे प्रिय लेखक रहे। मुझे उनका नाटक ‘जनमेजय का नागयज्ञ’ अपने व्यंग्यात्मक तेवर के कारण बहुत पसंद था/ है। उसी नाटक से मैंनें अपने लिए जनमेजय उपनाम पसंद किया तथा नरेंद्र कोहली से, एक पत्र द्वारा, इस उपनाम को रखने का परामर्श मांगा। उन्होंने स्वीकृति दी। प्रेम जनमेजय उपनाम से मैंनें पहली व्यंग्य रचना ‘राजधनी में गंवार’ अगस्त1969 लिखी जिसे मैनें लेखक-मंडल की गोष्ठी में पढ़ा। इस रचना को लगभग सबने पसंद किया, नरेंद्र कोहली ने भी परंतु कुछ किंतु-परंतु के साथ। ये पहली रचना थी जिसे मैंनें सरोजिनी नगर में टाईप सीखने जाने वाली दूकान में स्वयं हिंदी में टाईप भी किया। सन् 1968 में, शायद, आकाशवाणी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की- युवाओं के लिए ‘युववाणी’ कार्यक्रम का आरंभ। उस समय उसकी प्रोड्यूसर कमला संाघी थीं। बहुत ही सुलझी, समझदार और युवाओं को मदद करने को तत्पर। वो हर समय कुछ नया करने को प्रेरित करतीं। सन् 1969 में, शायद, कुमुद नागर ने आकाशवाणी ज्वाइन किया। वे नाटक देख रहे थे । मेरा उनसे परिचय युववाणी के कार्यक्रम में हुआ। उन दिनों वे युवाओं द्वारा लिखे गए, युवाओं की समस्याओं पर केंद्रित नए रेडियो नाटकों की तलाश में थे। उनकी प्रेरणा से मैंनें ‘दीवारें’ शीर्षक से पहला रेडियो नाटक लिखा जो 14 सितंबर 1969 को प्रसारित हुआ। बाद में मैंने पंाच छह -नाटक और लिखे जो उनके निर्देशन में प्रसारित हुए। उन दिनों हिंदी साहित्य में अनेक गुट विद्यमान् थे , अनेक हट्टियां खुली हुई थीं , अज्ञेय जैसे रचनाकार महंत की मुद्रा में थे । पूरा हिंदी साहित्य अनेक रूपों में सक्रिय था । धर्मयुग , साप्ताहिक हिुदंुस्तान , सारिका , नवनीत ,कल्पना, आधार , संचेतना , जैसी पत्रिकाओं ने साहित्यिक माहौल को गर्म किया हुआ था । इस सबका असर हिंदी विभाग के साहित्यकारों पर भी पडना ही था । दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी -साहित्य-सभा, विभाग में भी सक्रिय था। प्रो0 निर्मला जैन की सक्रियता ने ‘ मुट्ठियों में बंद आकार’ का प्रकाशन संभव बनाया। ये तत्कालीन सक्रिय गतिविधियों का असर था कि एक के बाद एक संकलन प्रकाशित हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी साहित्यिक सक्रियता की चर्मसीमा को दूने लगा। सन् 1965 से सन् 1975 के समय को यदि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का स्वर्णिम समय कहंू तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । आज हिंदी साहित्य में कृष्ण दत्त पालीवाल , सुधीश पचौरी , कर्ण सिंह चौहान , कमल कुमार ,दिविक रमेश ,प्रताप सहगल , सुरेश कांत , गोविंद व्यास अशोक चक्रधर ,हरीश नवल , सुरेश ऋतुपर्ण , अचला शर्मा,हरिमोहन शर्मा, महेशानन्द , सुरेश धींगडा , स्व0 मनोहर लाल , प्रताप सिंह , दिनेश ठाकुर, ओम गुप्त,रामकुमार,मीरा सीकरी ,शशि सहगल , आशा जोशी, पवन माथुर आदि का जो सशक्त साहित्यिक स्वर सुनाई दे रहा है , यह इसी काल का परिणाम है । उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तथा उससे संबंद्ध विभिन्न महाविद्यालयों के हिंदी विभाग में डॉ नगेंद्र , विजयेंद्र स्नातक , निर्मला जैन , सावित्री सिन्हा , मन्नु भंडारी, नित्यानंद तिवारी, इंद्र नाथ चौधुरी , अजित कुमार , महीप सिंह , रामदरश , मिश्र , नरेंद्र मोहन, नरेंद्र कोहली ,इंदु जैन , सुरेश सिन्हा , कैलाश वाजपेयी ,विश्वनाथ त्रिपाठी गंगा प्रसाद विमल , डॉ0 हरदयाल,विनय, ,स्नेहमयी चौधरी , पुष्पा राही, विनय आदि जैसे साहित्यिक व्यक्तित्व थे । उस समय हिंदी- विभाग की धरती बइुत उर्वर थी । उर्वर अब भी है पर कुछ और ‘पदार्थों’ के लिए। सुखबीर सिंह द्वारा संपादित ‘ दिविक ’ ने एक अजीब सी हलचल के साथ वातावरण को गर्म कर दिया । इस संकलन की योेजना ने नई पौध के अनेक नये रचनाकारों को एक जगह ला खड़ा किया । हिंदी साहित्य में इसका स्वागत भी हुआ । अनेक समीक्षकों नें इसे तार सप्तक- सा प्रयत्न भी माना । इसकी सफलता का श्रेय जहां सबमें बटना चहिए था वहां इसके व्यक्तिगत दावेदार अधिक हो गए । अज्ञेयी मुद्रा को धारण करने की चाह के कारण संभवतः सुखबीर सिंह अकेले से पड़ गए । संकलन की प्रसिद्धि ने सभी महंतों के मन में चाह भरी की एक संकलन उन्हें भी निकालना ही चाहिए । और यह इसी सोच का परिणाम था कि सुरेश ऋतुपर्ण नें ‘समीकरण ’ नामक कहानी संकलन संपादित किया जिसमें ऋतुपर्ण , प्रेम जनमेजय , अचला शर्मा , विजय सुषमा , हरीश नवल आदि छह कहानीकार थे । हिंदी विभाग के द्वारा ‘ मुट्ठियों में बंद आकार ’ प्रकाशित हुआ , ‘दूसरा दिविक ’ का संपादन सुखबीर सिंह और दिविक रमेश ने किया । सुखबीर सिंह द्वारा संपादित ‘दिविक ’का एक ऐतिहासिक महत्व और भी है । इस संकलन में एक कवि की कविताएं प्रकाशित हुई थीं , जिसका नाम था रमेश शर्मा । अदम्य आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ हरियाणा के गांव का यह छोरा सुखबीर सिंह को भा गया । मेरा परिचय इस रमेश शर्मा से अशोक चक्रध्र द्वारा संचालित‘प्रज्ञा’ की एक गोष्ठी में हुआ था, और बहुत जल्दी हम मित्र बन गए । मैं आरम्भ में प्रेम प्रकाश निर्मल के नाम से लिखा करता था , मैंने अपना उपनाम जनमेजय कर लिया । रमेश शर्मा भी अपने साथ किसी उपनाम की आवश्यकता अनुभव कर रहा था । उसने मुझसे सलाह ली कि अगर वह अपने नाम के साथ दिविक जोड़ ले तो कैसा रहेगा । वह थोडा हिचकिचा रहा था कि अन्य लोग इसको न जाने क्या अर्थ दे दें । मुझे दिविक रमेश नाम में कवित्व और एक नयेपन का अनुभव हुआ और मैने उसे अपनी सहमती दे दी । हो सकता है उसने इस संबंध में औरों से भी सलाह ली हो । दिविक रमेश नाम रखते ही वह चर्चा में आ गया । जैसी की उसे अपेक्षा थी लोगों में सुगबुबाहट हुई । कुछ ऐसे - वैसे कमेंट्स, दिमाग विहीन कवि जैसे, भी पीठ पीछे हुए , परन्तु सुखबीर के सहयोग और दिविक के अपने अदम्य साहस ने इसकी परवाह नहीं की । जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिविक के प्रकाशन ने एक सक्रियता उस समय के वातावरण में भर दी थी । साहित्य की राजनैतिक गतिविधयां आरम्भ हो गयीं । सन् 1970 में प्रकाशित इस संकलन में पंद्रह कवि थे , जिसका संपादन सुखबीर सिंह न किया था । और इसके पश्चात् जब 1973 के लगभग ‘दूसरा दिविक ’ नामक संकलन प्रकाशित हुआ , जिसका संपादन सुखबीर और दिविक रमेश ने किया । इस संकलन में सुखबीर और दिविक रमेश कांे छोडकर ‘दिविक ’ का कोई कवि नहीं था । इस संकलन मे मुझे भी कवि रूप में शामिल किया गया । इस संकलन की प्रस्तुति से ही स्पष्ट हो जाता है कि उस समय किस प्रकार की राजनीति हम लोगों के बीच पनप रही थी । अनजाने ही कुछ गुट जन्म ले रहे थे । सुरेश ऋतुपर्ण ने ‘ समीकरण’ निकाला तो उसमें दिविक और सुखबीर कहीं नहीं थे । दिविक ने कैलाश खोसला के साथ मिलकर ‘दिशाबोध ’ पत्रिका का संपादन आरम्भ कर दिया । मेरे और दिविक के सम्पादन में दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यंग्यकारो का पहला संकलन , ‘व्यंग्य एक और एक ’ के नाम से प्रकाशित हुआ । इसमें ग्यारह लेखकों की बाईस व्यंग्य रचनाएं थीं । दिल्ली विश्वविद्यालय के हस्तिनापुर कॉलेज, हिंदू कॉलेज और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज का मेरे साहित्यिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हस्तिनापुर कॉलेज ने जहां मुझे नरेंद्र कोहली, कैलाश वाजपेयी जैसे साहित्यिक गुरु दिए, वहीं हरिमोहन शर्मा, सुरेश कांत, राजेश कुमार, जोगेंद्र सिंह जैसे लेखक- मित्र भी दिए। हिंदू कॉलेज ने मुझे हरीश नवल तथा सुरेश ऋतुपर्ण जैसे तथा कॉलेज ऑपफ वोकेशनल स्टडीज ने रमेश उपाध््याय, हरीश नवल, विनय विश्वास, पूरबी पंवार, हरजेंद्र चौधरी, रत्नावली कौशिक जैसे लेखक-मित्र दिए। वोकेशनल कॉलेज में मैंनें और रमेश उपाध््याय ने एक ही दिन, 16 जुलाई 1973 को ज्वाईन किया। हरीश नवल वहां एक साल पहले से ही थे। हम तीनों की तिकड़ी जम निकली। हम तीनों अक्सर गोल मार्केट के आर्को या क्नॉट प्लेस के गलियारों में अक्सर घूमते । रमेश उपाध््याय उन दिनों बोरीबंदर के लाडले कथाकार कहे जाते थे। उनका साथ होने से मैं तत्कालीन अनेक साहित्यकारों से मिल पाया। हम तीनों ने वोकेशनल कॉलेज में अनेक साहित्यिक गोष्ठियों का संयोजन किया। धीरे-धीरे मेरा और रमेश उपाध्याय का साथ प्रगाढ़ होता गया। रमेश उपाध््याय ने सेठी पत्रिकाओं के विरोध में उठे आंदोलन का साथ दिया और एक विद्रोही तेवर अपनाया। रमेश उपाध््याय के साथ के कारण ही मैं प्रगतिशील साहित्य को समझ पाया और उस दृष्टिकोण को अपना पाया। रमेश उपाध््याय के कारण ही मेरी मित्रता चंडीगढ़ की साहित्यिक दुनिया से हुई। हम अक्सर ही विभिन्न साहित्यक गोष्ठियों में पंजाब के विभिन्न शहरों में साथ-साथ जाने लगे। मैं आभारी हूं कि रमेश उपाध््याय और दिविक रमेश की मित्रता ने मुझे साहित्य में प्रगतिशील परिवेश से परिचित करवाया और दृष्टिकोण-संपन्न किया। दिविक के कारण ही मैं जबलपुर में प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में गया, जिसकी अध्यक्षता परसाई जी ने की थी। उस सम्मेलन में जहां कुछ ‘उच्च’ प्रगतिशील लेखकों ने होटल में रुकना पसंद किया वहीं भीष्म साहनी जैसे जमीन से जुड़े रचनाकार ने हम जैसे तुच्छ लेखकों के साथ हॉल में, जमीन पर सोना बेहतर माना। वहां के अनुभव के आधार पर मैंनें बाद में एक व्यंग्य लिखा था-भेड़ाघाट,चांदनी रात और कवि मित्र’। धर्मयुग’ के ‘बैठे ठाले’ और ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ के ‘ताल बेताल’ स्तंभ में परसाई, त्यागी और जोशी का लगभग एकाधिकार था और ये तीनों हिंदी-साहित्य में व्यंग्य-त्रयी के रूप में प्रसिद्ध थे। वैसे हिंदी साहित्य का वह काल अनेक विधाओं में ‘त्रयी’ उपस्थिति के कारण त्रिगुणात्मक भी जाना जाता है। इन सब की व्यंग्य रचनाओं को पढ़ने के लिए इन पत्रिकाओं के ताजा अंक की प्रतीक्षा हमारी पीढ़ी के लोग उतनी ही शिद्दत से करते जितनी कि प्रेमिका की। अनेक बार ऐसा हुआ कि प्रेमिका तो समय देकर नहीं आई पर पत्रिका के अंकों ने वायदा निभाया। ये दीगर बात है कि जिनकी प्रेमिकाएं नहीं थी वे दूसरे की प्रतीक्षा देख प्रसन्न होते। ‘धर्मयुग’ मुख्य रूप से एक परिवारिक पत्रिका थी जिसमें इल्म से लेकर फिल्म तक, राजनीति से लेकर गृहनीति तक, सब प्रकाशित होता था। परंतु यह साहित्य क्षेत्र की सर्वप्रमुख पत्रिका थी। इसमें प्रकाशित होने वाली युवा लेखक की पहली प्रकाशित रचना उसे रातों रात साहित्य की दुनिया में चर्चित कर देती थी। इसमें प्रकाशित होना किसी भी युवा रचनाकार का स्वप्न होता था। मुझे याद है, मेरे समकालीन सुरेश ऋतुपर्ण की कविताएं रंग बिरंगे पृष्ठ में जब हम समकालीनों में सबसे पहले, प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई थीं तो हर युवा की यह प्रतीक्षा बन गई कि उसकी रचना ‘धर्मयुग’ में कब प्रकाशित होगी। मैंनें भी न जाने कितनी रचनाएं इस प्रतीक्षा में प्रकाशनार्थ ‘धर्मयुग’ में प्रेषित की परंतु अस्वीकृति के लिफाफों या प्रिंटेड पोस्टकार्ड का क्रम जारी रहा। फिल्मी विसंगतियों पर मेरे कुछ व्यंग्य टाइम्स ग्रुप की दूरी पत्रिका, जिसके संपादक अरविंद कुमार थे, अवश्य प्रकाशित हुए। मुझे याद है, जब मुझे मेरी पहली रचना का स्वीकृति कार्ड डाक से मिला तो उसे लेकर मैं नरेंद्र कोहली के घर ग्रेटर कैलाश गया था। उन दिनों मोबाईल तो क्या लैंडलाइंड फोन की सुविधा होना बड़ी बात थी। इसी ‘धर्मयुग’ ने जहां एक ओर मेरा परिचय हिंदी साहित्य जगत को दिया और मुझे और और अच्छा लिखने को प्रेरित किया वहीं दूसरी आर इसके संपादक धर्मवीर भारती ने मेरी लेखकीय महत्वाकांक्षा को सही दिशा दी। बात सन् 1984 की है। रामावतार चेतन उन दिनों हास्य-व्यंग्य की महत्वपूर्ण पत्रिका ‘रंग चकल्लस’ तो निकालते ही थे, उसकी बीसवीं वर्षगांठ पर उन्होंने ’चकल्लस पुरस्कार ट्रस्ट’ की स्थापना की जिसके अंतर्गत हास्य-व्यंग्य लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष बीस हजार रुपए का पुरस्कार विगत दस वर्षो की अवध् िमें हिंदी व्यंग्य साहित्य को सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिए जाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन भी होता था। रामावतार चेतन मंच की गरिमा के प्रति बेहद ही सावधान थे। कवि सम्मेलन के निमंत्राण के साथ निमंत्रित रचनाकार को निमंत्रण के साथ हिदायते भी संलग्न होती थीं। कवि सम्मेलन से एक दिन पहले बाकायदा रिहर्सल होती। मुझे 21 वें वार्षिक हास्य महोत्सव एवं चकल्ल्स पुरस्कार समर्पण समारोह के लिए बुलाया गया। इस समारोह में हरिशंकर परसाई को पुरस्कृत किया जाना था, ये दीगर बात है कि वे नहीं आ पाए। इस समारोह में जिन चकल्ल्सकारो को रचना पड़नी थी उनमें मेरे अतिरिक्त शरद जोशी, शैल चतुर्वेदी,आसकरण अटल, सुरेश उपाध्याय, विश्वनाथ विमलेश, अल्हड़ बिकानेरी, प्रदीप चौबे और मनोहर मनोज थे। 16 फरवरी को बाकायदा रिहर्सल थी जिसमें रामावतार चेतन ने मुझे शरद जोशी के हाथ सौंप दिया। शरद जोशी ने मेरी तीन रचनाओं में से ‘जाना पुलिस वालों के यहां इक बारात में’ व्यंग्य पाठ के लिए चुनी। कुछ टिप्स दिए। ये मेरे लिए किसी बड़े मंच पर व्यंग्य पाठ करने का पहला अवसर था। परीक्षा की घड़ी जैसा। इस मंच पर मुझे और शरद जोशी को गद्य-व्यंग्य पाठ करना था। यह मेरी लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। अगले दिन, 17 पफरवरी को, कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट व्यक्तिओं में धर्मवीर भारती भी थे। मेरी रचना बहुत जमी। शरद जोशी ने अंत में अपनी दूसरी रचना भी पढ़ी। अगले दिन मैं भारती से मिलने ‘धर्मयुग’ के दफतर गया। भारती जी ने अपने लिए नींबू वाली चाय और मेरे लिए सामान्य चाय मंगवाई। बीस-पच्चीस मिनट तक उनसे अनेक विषयों पर बातचीत हुई, विशेषकर परसाई जी को लेकर। इस बातचीत में मेरा युवामन निरंतर इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि भारती जी, पिछले दिन मेरे द्वारा किए गए सफल व्यंग्य पाठ पर, कुछ प्रशंसात्मक कहेंगें, मेरी पीठ ठोकेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब लगा कि बातचीत समाप्त होने के दौर में है तो मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंनें दोनों हाथेलियों को एक दूसरे के साथ विवशता में मलते हुए कहा- भाई सहब, कल का मेरा व्यंग्य-पाठ आपको कैसा लगा?’ भारती जी थोड़ा मुस्कराए, बोले- बढ़िया था,’ फिर थोड़ी देर रुके और बोले,‘देखो प्रेम, तुम दोराहे पर हो,यहां से तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं- एक तालियों भरा मंच का रास्ता है जिसमें पैसा है और तुरंत यश पाने का सरल मार्ग है, और दूसरा वो रास्ता है जिसपर तुम अभी चल रहे हो तथा जो लंबा और कठिन है। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है।’ - पर भाई साहब, शरद जोशी भी तो मंच से जुड़े हैं और...’ - प्रेम, पहले शरद जोशी बन जाओ।’ मेरे लिए यह मंत्र बहुत था। इसके बाद मंच मेरी कभी प्राथमिकता तो क्या प्रलोभन भी नहीं रहा। मंच को अछूत नहीं समझा, उससे घृणा नहीं की, पर मंच के लिए कभी लालायित नहीं रहा। ‘चकल्लस’ कार्यक्रम के बाद शरद जी से मेरा निरंतर संपर्क रहा। मेरे लिए वो दिन चिरस्मरणीय है जिस दिन शरद जोशी मेरे नौरोजी नगर वाले निवास पर आए थे और उस दिन रवींद्रनाथ त्यागी, नरेंद्र कोहली भी साथ थे। वैसे तो शरद जोशी होने के अनेक अर्थ हैं पर सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि वे जीवन भर अनर्थ के विरुद्ध लड़ते रहे । गलत के विरुद्ध लड़ने के लिए उनके हथियार अपने थे और इन हथियारों के प्रयोग के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और न ही इस बात की चिंता थी कि उनका आका इस बात पर उनकी पीठ थपथपाएगा कि नहीं क्योंकि उनका कोई आका था ही नहीं । और यदि कोई आका था भी तो वो उनका पाठक वर्ग था, जिसने उनकी सदा ही पीठ थपथपाई। यही कारण है कि शरद जोशी ने अपने समय के यथार्थ का यथार्थ के धरातल पर ही निरीक्षण परीक्षण किया है । व्यंग्य-लेखन अपने आरंभिक दौर में व्यंग्य लेखन की प्रेरणा मैंने नरेंद्र कोहली के अतिरिक्त परसाई, जोशी और त्यागी की त्रयी से ली। अपने अग्रज व्यंग्यकारों का मुझे पर्याप्त मार्गदर्शन और स्नेह मिला। इन व्यंग्यकारों को मैंने चाव से पढ़ा और इनकी अपनी-अपनी अलग लेखन शैली से प्रभावित भी हुआ। व्यंग्य की इस त्रयी में से आरंभ में मेरी पर्याप्त निकटता रवीन्द्रनाथ त्यागी से तथा बाद में इस त्रयी के चौथे महत्वपूर्ण स्तम्भ श्रीलाल शुक्ल जी से रही। परसाईजी जब अपनी टांग के इलाज के लिए, सन् 1976 में, सपफदरजंग में भरती हुए थे, उन दिनों मैं पास में, नौरोजी नगर में रहता था, परसाईजी से अनेक मुलाकातें हुई और परसाई की आत्मीयता ने मुझे वशीभूत कर दिया। यह मुलाकाते मेरे लेखकीय जीवन को सही ‘शेप’ देने में प्रमुख सहायक हुईं। इनही मुलाकातों के दौरान मैंनें और हरिमोहन शर्मा ने ‘सार्थक’ पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की जिसमें परसाई ने कहा कि प्रेम हमनें अपने पिता को नंगा नहीं देखा, तुम्हारी पीढ़ी देख सकती है।परसाई जी की आत्मीयता ने तो मुझे जैसे उनका दीवाना बना दिया। 25 सितंबर 1976 को मेरे बड़े बेटे उज्ज्वल का पहला जन्मदिन था और वह मेरे निवास एफ-64 नौरोजी नगर में मनाया भी गया। उस उपलक्ष्य में मैं अगले दिन मिठाई लेकर परसाई जी के पास अस्पताल गया। उन्होंनें न केवल बड़े चाव से मिठाई खाई अपितु जबलपुर लौटने पर अपने 09-02-1977 के पत्र में लिखा- पांव का हाल यह है कि अब धीरे-धीरे बिना सहारे के चल लेता हूं। सड़क पर आनें में अभी समय लगेगा। लिखना अब शुरु कर दिया है। अरसे से छूटा हुआ था। अभी तो देश की राजनीति के चमत्कार ही इतने हैं कि उन्हें समझने में ही समय निकल जाता है।... दिल्ली के अस्पताल में मुझे प्राणांतक मानसिक त्रास होता अगर आप सब न होते। सब मित्रों को मेरा नमस्कार कहें।आपका बच्चा जिसके जन्मदिन की मिठाई मैंनें खाई थी, मजे में होगा।’ सितंबर में खाई मिठाई को फरवरी तक याद रखना और मेरे उस बेटे के मजे में होने का आर्शीवाद - सा देना... कौन न अभिभूत होगा ऐसी आत्मीयता के प्रति। परसाई ने 1977 में देश की राजनीति के जिस चमत्कार की चर्चा की है, उससे हमारी पीढ़ी तो परिचित ही होगी। मैंनें भी आपात्काल की विसंगतियों को लक्षित कर दो व्यंग्य लिखे थे। ‘लेखकीय पीड़ा के पांच दिन’ ‘धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था जिसपर अन्य प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ नागार्जुन जी की प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया भी मिली थी और दूसरा व्यंग्य ‘नेकरों की वापसी’ शीर्षक से ‘जनयुग’ में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ के जबलपुर में आयोजित सम्मेलन के दौरान तथा जब भी जबलपुर जाना हुआ उनसे मिलना एक आवश्यक कार्य बन जात। परसाई जी के व्यक्तित्व में अपने से बाद की पीढ़ी के लिए एक चुंबकीय असर था। लेखन के क्षेत्र में कोई कितना भी नया हो परसाई उसे कभी छोटा अनुभव नहीं होने देते थे। सार्थक व्यंग्य लेखन का संस्कार मैंने उन्हीं से ग्रहण किया। रवीन्द्रनाथ त्यागी अपने से बाद की पीढ़ी से जुड़ने को सदा तत्पर रहते थे। अपने से बाद की पीढ़ी को न सिर्फ पढ़ना अपितु गंभीरता से उनकी रचनाओं का विश्लेषण करना और बेबाकी से अपनी राय देनाµ उनके इस साहित्यिक व्यक्तित्व ने अनेक युवा रचनाकारों से अनायास ही आत्मीय संबंध् बना लिए। उम्र में अपने से बहुत ही छोटे रचनाकारों को अपनी पुस्तक समर्पित कर देना उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा गुण है जो बहुत कम देखने में आता है, वरना तो समर्पण करते समय अनेक गणित लगाए जाते हैं। ‘कंट्रोल ऑफ डिपफेंस एकाउंटस’ होने के बावजूद वे इस गणित से अपरिचित थे। उनके व्यक्तित्व में आत्मीय संबंधें की एक अतृप्त प्यास दिखाई देती है। जिससे एक बार संबंध बन गया, उसमें नारजगी तो आ सकती है पर टूटन नहीं। एक बात और जिसने मुझे रवीन्द्रनाथ त्यागी से निरंतर जोड़े रखाµ वे संबंधें को न तो कैश करते थे और न किसी को कैश करने देते थे। आपके आत्मीय हैं और आत्मीयता में स्वयं को उड़ेल भी देंगे, परंतु आपकी खराब रचना को सिरे से खारिज करने से हिचकिचाएंगे नहीं। श्रीलाल शुक्ल के साहित्य और व्यवहार ने एक संत की तरह मुझे अपनी बेबाक राय दी है। श्रीलाल जी से तो मेरा संपर्क एक संयोग ही था और उस संपर्क से पहले मैं उनके लेखन से चमत्कृत ही था। श्रीयुत् श्रीकृष्ण के ‘पराग प्रकाशन’ के लिए बीसवीं शताब्दीः व्यंग्य’ का संपादन करते हुए मैंंने श्रीलाल जी से उनकी एक रचना का आग्रह किया। वे दिल्ली अपने शेख सराय वाले घर में आए हुए थे और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। ‘राग दरबारी’ के लेखक से पहली बार मिलना मेरे लिए सुंदर स्वप्न-सा ही था। मैं लगभग अवाक् उनके कहे को सुन रहा था। ये मेरे अति निम्न मध्यवर्गीय जीवन परिवेश जनित हीन भावना का परिणाम है कि अपने से श्रेष्ठ के सामने जाते ही मेरा आधा बल उसके पास चला जाता है और मस्तिष्क जैसे शून्य हो जाता है, अवाक् की स्थिति आ जाती है। बहुत परिश्रम से मैं अपने आपको इस स्थिति से निकाल पाता रहा हूं। चार वर्ष तक विदेश में विदेश मंत्रालय के सहयोगियों के साथ रहने पर अब स्थिति कुछ भिन्न हो गई है। श्रीलाल जी ने बताया कि वे नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन का संपादन कर रहे हैं, पर काम बहुत समय ले रहा है, यदि मैं उनकी इसमें सहायता करूं तो उन्हें प्रसन्नता होगी। श्रीलाल जी के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य था, चाहे बेगार ही क्यों न हो। पर वो बेगार नहीं थी- मेरे हां कहने पर उन्होंने तत्काल कहा कि वे नेशनल बुक ट्रस्ट को इस विषय में पत्र लिख देंगे और मैं उनके साथ दूसरे संपादक के रूप में रहूंगा। इस संत स्वभाव ने मुझे प्रभावित किया और एक ऐसा सत्संग दिया जिसने साहित्य और जीवन की समझ दी। हास्य-व्यंग्य सकलन की तैयारी के दौरान श्रीलाल जी से बहुत मुलाकातें हुई जिनके कारण मैं जान पाया कि नामवर सिंह ने कुछ उत्कृष्ट व्यंग्य लिखे हैं, कि गोपालप्रसाद व्यास ने कविता की अपेक्षा गद्य में अच्छी रचनाएं लिखी हैं कि जहां कुछ लोग अपने लिए विवाद क्रिएट करते हैं वहां श्रीलाल जी विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं वरना संकलन तैयार करते समय उनके पास अनेक ऐसे अवसर थे परंतु उन्होंने मुझे भी विवाद से दूर रहने की सलाह दी, कि. . .ऐसे ‘कि’ बहुत हैं और जो एक लंबे आलेख का विषय हैं। धीरे-धीरे मैं श्रीलाल जी करीब आया, उनके साथ रसरंजनमय कुछ शामें भी व्यतीत कीं। साहित्य के प्रति उनकी गहरी समझ ओर अध्ययनशील व्यक्तित्व से मैंने बहुत कुछ सीखा। वे बहुत सजग हैं और हम्बग से चिढ़ के कारण वे लाग लपेट में विश्वास नहीं करते हैं। वे बातचीत में बहुत जल्दी अपनी आत्मीयता को सक्रिय कर देते हैं। अपने लेखकीय व्यक्तित्व की एकरूपता को वे तोड़ते रहे हैं। ऐसे में जब अधिकांश साहित्यकार स्वयं को एक प्रफेम में बंधे होता देख प्रसन्न होते हैं वे अपनी अगली कृति में अपने पिछले फ्रेम को तोड़ते दिखाई देते हैं। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रश्नचिह्न लगाते हैं। उनका लेखन एक चुनौती प्रस्तुत करता है। आप उन पर कुछ भी सतही कहकर किनारा नहीं कह सकते हैं। वे विनम्र हैं पर ऐसी संतई विनम्रता नहीं कि आप इसे उनकी कमजोरी मान लें। मेरा पहला संग्रह, ‘राजधानी में गंवार’ 1978 में पराग प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था और वह भी श्रीकृष्ण ;भगवान नहीं, प्रकाशक की कृपा से। उन दिनों के चर्चित युवा कवि एवं चित्रकार अवध्ेाश ने इसका कवर बनाया था। हरीश नवल पुराने मित्र, कॉलेज में सहयोगी और व्यंग्य लेखन के पुराने सहयात्री हैं। उन्होंने पुस्तक पर गोष्ठी का आयोजन किया, वह भी मुफ्रत में। कार्ड भी भाई श्रीकृष्ण ने छपवा दिए थे और अध्यक्ष, मुख्य अतिथि वक्ता और श्रोता बिना मार्ग व्यय लिए आ गए। हां कार्ड बांटने के लिए मैंने पूरी दिल्ली का चक्कर लगाया था पर मैं अकेला नहीं था मेरे साथ मेरे स्कूटर के पीछे उस समय का चर्चित युवा व्यंग्यकार अंजनी चौहान था जिससे न जाने क्यों मैं आतंकित था। गर्मियों की दोपहर में अंजनी चौहान ने मेरे साथ कार्ड बांटे पर जिस दिन गोष्ठी थी उससे एक दिन पहले दिल्ली से गायब हो गया और भोपाल भाग गया। हरीश नवल के राणा प्रताप बाग के ड्राईंग रूम में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता रवीन्द्रनाथ त्यागी ने की थी और उसमें अवधनारायण मुद्गल, रमेश उपाध्याय, दिविक रमेश, रमेश बतरा, शेरजंग गर्ग, हरदयाल, डॉ0 विनय, बलराम, विनय, हरीश नवल, राजा खुगशाल, सुभाष अखिल,आदि अनेक साहित्यकार उपस्थित थे। मुझे सोचकर अच्छा लगता है कि इसके बाद मेरे विभिन्न संकलनों का लोकार्पण त्रिलोचन,नामवर सिंह, विजयेंद्र स्नातक, कन्हैयालाल नंदन, निर्मला जैन, कमलेश्वर आदि ने किया। ज्ञान चतुर्वेदी का आजकल मेरे साहित्यिक और व्यक्तिगत जीवन में विशेष दखल है। यह दखल एकदम प्रविष्ट नहीं हुआ है अपितु सहज पके सो मीठा होए कि शैली में विकसित हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के लेखन को धर्मयुगीय समय से चीह्नते रहे हैं । हम दोनों को एक कड़ी में जोड़ने वाला, हमारे समय का तीखे तेवर वाला बेबाक व्यंग्यकार अंजनी चौहान था। अंजनी चौहान का ऐसा व्यक्तित्व रहा हे कि उसके सामने अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाए। आरंभ में मेरी दोस्ती अंजनी के साथ जमकर थी। उसी के माध््यम से मुझे ज्ञान का पहला संकलन श्रीकृष्ण से प्रकाशित करवा देने के लिए मिला था। मैंनें उस संकलन के बारे में श्रीकृष्ण से बात की और उन्होंने मेरी ‘विनती’ स्वीकार भी की। वही सूचना मैंनें ज्ञान को भी दे दी। श्रीकृष्ण प्रकाशक थे और मैं अकिंचन नया लेखक, कितना प्रभावशाली हो सकता था? समय गुजरता गया, बार-बार की पूछताछ के बाद प्रकाशक से उत्तर न मिला, पर उधर गलतफहमियां पैदा होने लगीं। मेरे पास आज भी ज्ञान के वो पत्र हैं जहां वो मुझपर शक करता हुआ देखा जा सकता है। अंजनी को लगा कि पानी सर से उतर गया है और उसने ज्ञान का संकलन अपने बूते पर प्रकाशित किया। गलतफहमी में घी पड़ा और उसके भाई बंधु भी पैदा हो गए। पर ज्ञान में एक बहुत बड़ी खूबी है, वो गलतफहमी को अधिक नहीं लादता है। धीरे-धीरे एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ीं, और आज हम एक दूसरे को शायद अपने से अधिक समझते हैं। ज्ञान दिल्ली आए और मुझे न मिले या मैं भोपाल जाउं और उससे न मिलूं, हो नहीं सकता। आयोजकों की रहने की व्यवस्था होने के बावजूद हम एक दूसरे के घर रहना पसंद करते हैं। ज्ञान हमारी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है। उसने ‘राग दरबारी’ के आतंक को तोड़ा है। उसने व्यंग्य लेखन से जुड़े अनेक मिथ तोड़े हैं। धरावाहिक लेखन का दौर मेरे और हरीश नवल के जीवन का गजब - अजब दौर रहा। पहले इसने गजब तरह से हमें इस चकाचौंधमय दुनिया की सुनहरी गलियों की सैर करवाई और फिर इस दुनिया के अजब लोगें की अजब हरकतों ने, विशेषकर मुझे, यह गाने मेरा परिवार
परदादा
स्व0 श्री खेमामल कुंद्रा दादा स्व श्री अमरचंद कुंद्रा
पिता
स्व0 श्री राम प्रकाश कुंद्रा जन्म-21-7-1921, स्वर्गवास 31-12-2002 सी ए जी दफतर में र्क्लक माता स्व0 श्रीमती सत्या कुंद्रा जन्म वर्ष 1926 स्वर्गवास 8-8-2008 घरेलू महिला भाई सत्य प्रकाश कुंद्रा जन्म 22-3-1951, हरियाण टूरिजम से पदमुक्त,
शांति प्रकाश कुंद्रा जन्म 13-8-1953 स्वराज माजदा में प्रबंधक
पत्नी आशा जन्म 10-11-1950 दिल्ली सरकार के विद्यालय में संस्कृत पी जी टी पुत्र उज्ज्वल जन्म 25-9-1975, एरिसेंट,गुड़गांव में सीनियर एक्जेक्यूटिव
विदित जन्म 21-12-1980, प्राणा स्टूडियोज ,मुम्बई, में सीनियर ग्राफिक
पुत्रावधू अभिलाषा जन्म 01-04-1976 मारुति कंपनी,गुड़गांव, में प्रबंधक
नेहा जन्म 13-07-1981मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज,मुम्बई, में सीनियर
एक्जेक्यूटिव
पौत्र रुचिर जन्म 08-07- 2003
हिमांक जन्म 25-09-2008
मेरा बचपनUnder Construction मेरा विद्यालयUnder Construction मेरा विश्वविद्यालयUnder Construction मेरे मित्रUnder Construction संगोष्ठियों में भागीदारी
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में
भागीदारी
• साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक संबंध परिषद् एवं अक्षरम् के संयुक्त तत्वावधन में आयोजित ‘प्रवासी हिंदी उत्सव -2006’ एवं 2007 की अकादमिक समिति के संयोजक
• वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय, हिन्दी निधि तथा भारतीय
उच्चायोग द्वारा त्रिनिडाड में 17 से 19 मई 2002 तक आयोजित
त्रिदिवसीय ‘ अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन ’ के आयोजन में
अकादमिक - समिति के अध्यक्ष तथा आयोजन समिति के सदस्य के रूप
में महत्वपूर्ण भूमिका ।
• यू0के0, न्यू जर्सी , मिआमी , वेस्ट इंडीज और भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आलेख पाठ एवं चर्चाओं में अध्यक्षता, आलेख पाठ एवं भागेदारी ।
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन
• दिल्ली विश्वविद्यालय तथा रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा आयोजित ‘ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ’ में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान ।
• लखनउ, चंडीगढ , भोपाल , रायपुर, दुर्ग, हरदा , बरेली
, राजमहेंद्री , जालंध्र, बम्बई , बडौदा , कलकता
,जयपुर,उदयपुर, जबलपुर , इलाहाबाद , इंदौर , गंज
बसौदा गाजियाबाद , दिल्ली, शहडोल, जमशेदपुर आदि नगरों की
साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आयोजित साहित्यिक गोष्ठियों तथा
सम्मेलनों की अध्यक्षता / रचना पाठ / आलेख पाठ ।
• हिंदी की सभी शीर्ष पत्रा -पत्रिकाओ, र्ध्मयुग,
सारिका, दिनमान, पराग, नवभारत टाईम्स, शकर्स वीकली आदि में
लगभग दो सौ रचनाएं प्रकाशित ।
• दूरदर्शन’ के लिए धरावाहिकों का लेखन अनेक साहित्यिक
कार्यक्रमों में भागेदरी
• आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण से अनेक नाटक प्रसारित
।
• अनेक रचनाओं का अंग्रेजी , पंजाबी,गुजराती तथा मराठी
में अनुवाद ।
|